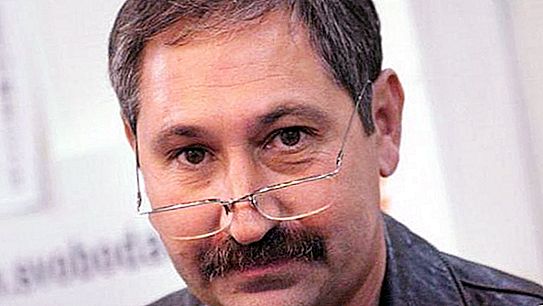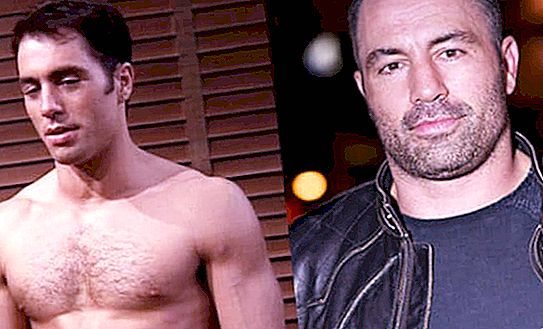जो चीज हमें घेरती है, उसके बारे में जिज्ञासा यह समझने का प्रयास करती है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, साथ ही साथ दूसरी दुनिया के अज्ञात संसार में प्रवेश करने की इच्छा भी हमेशा से मानव मन की निशानी रही है। जब लोग ऐसा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं या दूसरों के साथ हो रहे कुछ का निरीक्षण करते हैं, तो वे इसे आत्मसात करते हैं और इसे समेकित करते हैं, न केवल यह समझना चाहते हैं कि मामलों की स्थिति क्या है, बल्कि यह भी कि क्या सच को समझना संभव है। दर्शन में अनुभूति सबसे दिलचस्प प्रश्नों में से एक है, क्योंकि दर्शन मानव मस्तिष्क में होने वाली विविध प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने और समझाने की कोशिश कर रहा है और इसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है।
ज्ञान के संचय की तुलना में अनुभूति की प्रक्रिया अधिक जटिल है - यह रचनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक है; इसमें न केवल तर्कसंगत, बल्कि सोच का सहज और संवेदी तंत्र शामिल है। इसीलिए दर्शनशास्त्र में अनुभूति एक विशेष समस्या है, जो एक विशेष सैद्धांतिक खंड से संबंधित है जिसे एपिस्टेमोलॉजी या एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। दर्शन की एक विशेष शाखा के रूप में महामारी विज्ञान की शुरुआत 19 वीं शताब्दी में स्कॉट फेरियर द्वारा रखी गई थी। यह दार्शनिक अनुशासन ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों और सिद्धांतों दोनों का अध्ययन करता है, साथ ही साथ अनुभूति क्या है, इसका वास्तविक दुनिया के साथ क्या संबंध है, क्या इसकी सीमाएँ हैं, और यह भी कि जो जानते हैं और जो जानते हैं, उनके बीच क्या संबंध हैं। ज्ञान के कई अलग-अलग सिद्धांत हैं जो एक-दूसरे की आलोचना करते हैं और इस बारे में कई अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं कि ज्ञान क्या सत्य और विश्वसनीय है, इसके प्रकार क्या हैं और क्यों हम आम तौर पर दुनिया और खुद को जानने में सक्षम हैं।
संक्षेप में, क्षेत्र में दार्शनिक यह समझने के लिए चिंतित हैं कि ज्ञान क्यों मौजूद है; हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि यह ठीक ज्ञान है जिसमें निश्चितता और सच्चाई है, और सतही निर्णय (या राय), या भ्रम भी नहीं है; यह ज्ञान कैसे विकसित होता है, और यह भी कि अनुभूति के तरीके क्या हैं। दर्शन में, अपने पूरे इतिहास में, यह सवाल मनुष्य और मानवता के लिए ज्ञान के अधिग्रहण के अर्थ के बारे में अत्यंत तीव्र है, चाहे वह खुशी या दुख लाए। लेकिन जैसा कि यह है कि आधुनिक समाज के जीवन में, नए ज्ञान के अधिग्रहण ने इतना महत्व हासिल कर लिया है कि इस समाज के विकास के वर्तमान चरण को अक्सर सूचनात्मक कहा जाता है, खासकर जब से यह सूचनात्मक स्थान है जिसने मानवता को एकजुट किया है।
दर्शन में अनुभूति एक ऐसी प्रक्रिया की तरह दिखती है जिसमें सामाजिक, मूल्य प्रकृति होती है। इतिहास बताता है कि लोग न केवल नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार थे, बल्कि इसे बनाए रखने के लिए भी थे, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें अक्सर, और अब अपने जीवन, स्वतंत्रता, रिश्तेदारों से अलगाव के साथ भुगतान करना पड़ता है। चूंकि यह एक प्रक्रिया है, यह दर्शन में अध्ययन की गई अन्य प्रकार की गतिविधियों के समान है, और उनकी तरह, जरूरतों (इच्छा को समझने, समझाने), उद्देश्यों (व्यावहारिक या विशुद्ध बौद्धिक), लक्ष्यों (ज्ञान प्राप्त करना, सच्चाई की समझ) से निर्धारित होता है, का अर्थ है (जैसे अवलोकन, विश्लेषण, प्रयोग, तर्क, अंतर्ज्ञान और इतने पर) और परिणाम।
मुख्य समस्याओं में से एक दार्शनिक विचार में रुचि है कि अनुभूति कैसे विकसित होती है। दर्शनशास्त्र ने शुरू में स्थापित किया था कि पहले प्रकार का ज्ञान भोला, सामान्य ज्ञान था, जो समय के साथ, संस्कृति के विकास की प्रक्रिया में सुधार हुआ, जिससे वैज्ञानिक ज्ञान और सोच के सैद्धांतिक सिद्धांतों का उदय हुआ। इसी समय, दर्शन दार्शनिक ज्ञान के सिद्धांतों और विधियों के बीच अंतर करता है और विशिष्ट वैज्ञानिक ज्ञान (विज्ञान के दर्शन) का अध्ययन करता है।
दार्शनिकों ने यह भी सोचा कि अनुभूति की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विषय क्या भूमिका निभाता है। दर्शन में अनुभूति न केवल किसी व्यक्ति के आस-पास की चीजों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है या स्वतंत्र रूप से होती है, बल्कि उसका आध्यात्मिक जीवन भी होता है। जानकर, एक व्यक्ति को न केवल यह एहसास होता है कि वह किसी बाहरी चीज का अध्ययन कर रहा है, बल्कि यह भी कि यह अध्ययन खुद को प्रभावित करता है। इसके अलावा, विशेष रूप से मानवीय अनुभूति के क्षेत्र में, जानने वाले विषय की स्थिति, उसके मूल्य और विश्वास अनुभूति के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इस जटिल समस्या का आकलन करते हुए, विभिन्न दिशाओं के दार्शनिक पूरी तरह से विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचे। उदाहरण के लिए, प्रत्यक्षवादियों ने वस्तुनिष्ठता की कमी के लिए मानवीय ज्ञान को ठेस पहुंचाई, और दार्शनिक धर्मशास्त्र के प्रतिनिधियों ने, इसके विपरीत, विषयवस्तु को मानवीय ज्ञान की एक विशिष्ट विशेषता माना, जो कि, इस तरह से सच्चाई के करीब है, और, इस प्रकार, सत्य के लिए।